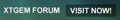



नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय पांच उप-प्राण हैं।
प्राण का कार्य श्वसन है; अपान उत्सर्जन करता है; समाना पाचन क्रिया करता है; उदान भोजन को निगलने का काम करता है। इससे जीव को नींद आ जाती है। यह मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से अलग करता है। व्यान रक्त का संचार करता है।
नागा को डकारें और हिचकी आती है। कूर्म आंखें खोलने का कार्य करता है। क्रिकारा भूख और प्यास उत्पन्न करता है। देवदत्त जम्हाई लेता है। धनंजय मृत्यु के बाद शरीर के विघटन का कारण बनता है। वह मनुष्य कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेता, चाहे उसकी मृत्यु कभी भी हो, जिसकी श्वास ब्रह्मरंध्र को भेदकर सिर से बाहर निकल जाती है।
प्राण को रक्त, लाल मणि या मूंगा के रंग का बताया गया है। बीच में जो अपान है, वह इन्द्रगोप (सफेद या लाल रंग का एक कीट) के रंग का है। समान का रंग शुद्ध दूध या क्रिस्टल के बीच का या तैलीय और चमकदार रंग का होता है, अर्थात प्राण और अपान दोनों के बीच का कुछ। उदान अपांडुरा (हल्के सफेद) रंग का है और व्यान का, आर्चिल (या प्रकाश की किरण के रंग) जैसा दिखता है।
वायु के इस पिंड की मानक लंबाई 96 अंक (6 फीट) है। साँस छोड़ते समय वायु-प्रवाह की सामान्य लंबाई 12 अंक (9 इंच) होती है। गाने में इसकी लंबाई 16 अंक (1 फुट), खाने में 20 अंक (15 इंच), सोने में 30 अंक (22 1/2 इंच), मैथुन में 36 अंक (27 इंच) और शारीरिक व्यायाम करने में हो जाती है। यह उससे कहीं ज़्यादा है। समाप्ति वायु-धाराओं की प्राकृतिक लंबाई (9 इंच से) कम करने से जीवन लम्बा हो जाता है और धारा बढ़ने से जीवन की अवधि कम हो जाती है।
प्राण को बाहर से अंदर लेते हुए, उससे पेट भरकर, प्राण को मन के साथ, नाभि के मध्य में, नाक की नोक पर और पैर की उंगलियों पर, संध्या के दौरान (सूर्योदय और सूर्यास्त) या समय पर केन्द्रित करें। सभी समय। इस प्रकार योगी सभी रोगों और थकान से मुक्त हो जाता है। इस प्राण को नाक की नोक पर केन्द्रित करके वह वायु के तत्वों पर प्रभुत्व प्राप्त करता है; उसकी नाभि के मध्य में केन्द्रित होने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं; पैर की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करने से उसका शरीर हल्का हो जाता है। जो जीभ से वायु पीता है, उसकी थकान, प्यास तथा अन्य अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तीन महीने के भीतर दो संध्याओं और रात्रि के अंतिम दो घंटों में अपने मुख से वायु पीता है, उसके वाक् (वाणी) में शुभ सरस्वती (वाणी की देवी) मौजूद रहती है, अर्थात वह वाक्पटु हो जाता है और सीखा। छह माह में वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जिह्वा के मूल में वायु को खींचकर अमृत पीकर बुद्धिमान व्यक्ति समस्त समृद्धि का आनंद लेता है।
यहां फेफड़ों और उनके कार्यों पर एक शब्द का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। श्वसन के अंगों में दो फेफड़े होते हैं, एक छाती के दोनों ओर और वायु मार्ग जो उन्हें ले जाता है। वे छाती की ऊपरी वक्षीय गुहा में मध्य रेखा के प्रत्येक तरफ एक-एक स्थित होते हैं। वे हृदय, बड़ी रक्त वाहिकाओं और बड़ी वायु-नलिकाओं द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। फेफड़े स्पंजी, छिद्रपूर्ण होते हैं और उनके ऊतक बहुत लचीले होते हैं। फेफड़ों के पदार्थ में असंख्य वायु-कोष होते हैं, जिनमें वायु होती है। पोस्टमार्टम के बाद जब इसे पानी के बेसिन में रखा जाता है तो यह तैरने लगता है। वे फुस्फुस नामक एक नाजुक सीरस झिल्ली से ढके होते हैं जिसमें सांस लेने की क्रिया के दौरान फेफड़ों के घर्षण को रोकने के लिए सीरस द्रव होता है। फुस्फुस का आवरण की एक दीवार फेफड़ों से निकटता से चिपकी होती है। दूसरी दीवार छाती की भीतरी दीवार से जुड़ी हुई है। इस झिल्ली के माध्यम से फेफड़े छाती की दीवार से जुड़े होते हैं। दाहिने फेफड़े में तीन लोब होते हैं। बाएँ फेफड़े में दो लोब होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में एक शीर्ष और एक आधार होता है। आधार को डायाफ्राम, मांसपेशी सेप्टम, गले और पेट के बीच की विभाजन दीवार की ओर निर्देशित किया जाता है। शीर्ष ऊपर स्थित है, गर्दन की जड़ के पास। यह वह आधार है जो निमोनिया में सूज जाता है। फेफड़ों के शीर्ष भाग को ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति नहीं मिलती है, जो खपत से प्रभावित होता है। यह ट्यूबरकल बेसिली (टीबी) के लिए अनुकूल निडस या प्रजनन भूमि प्रदान करता है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम और गहरी सांस लेने के अभ्यास से, इन शीर्षों को ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति मिलती है और इस प्रकार यक्ष्मा रोग से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम से फेफड़ों का विकास होता है। जो प्राणायाम का अभ्यास करता है उसकी आवाज शक्तिशाली, मधुर और सुरीली होती है।
वायु-मार्ग में नाक, ग्रसनी या गले, स्वरयंत्र या वायु बॉक्स, या ध्वनि बॉक्स का आंतरिक भाग शामिल होता है, जिसमें दो स्वर रज्जु, श्वासनली या श्वासनली होती है: दाहिनी और बाईं ब्रांकाई और छोटी ब्रोन्कियल नलिकाएं। जब हम सांस लेते हैं, तो हम नाक के माध्यम से हवा खींचते हैं और ग्रसनी और स्वरयंत्र से गुजरने के बाद, यह श्वासनली या श्वासनली में गुजरती है, वहां से दाएं और बाएं ब्रोन्कियल ट्यूबों में जाती है, जो बदले में असंख्य छोटी ट्यूबों में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है। ब्रोन्किओल्स, और जो फेफड़ों की छोटी वायु-थैलियों में सूक्ष्म उपविभाजनों में समाप्त होते हैं, जिनमें से फेफड़ों में लाखों होते हैं। फेफड़ों की वायु-थैलियाँ जब एक अखंड सतह पर फैलती हैं, तो 1,40,000 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर कर लेंगी।
डायाफ्राम की क्रिया द्वारा हवा फेफड़ों में खींची जाती है। जब इसका विस्तार होता है, तो छाती और फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है और बाहरी हवा इस प्रकार बने निर्वात में चली जाती है। छाती और फेफड़े सिकुड़ते हैं, जब डायाफ्राम शिथिल हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है।
स्वरयंत्र में स्थित स्वर रज्जुओं के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वरयंत्र ध्वनि बॉक्स है। जब गायन और लगातार व्याख्यान देने जैसे स्वर रज्जुओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, तो आवाज कर्कश हो जाती है। महिलाओं में ये डोरियाँ छोटी होती हैं। इसलिए उनकी आवाज मधुर है। प्रति मिनट श्वसन की संख्या 16 है। निमोनिया में यह बढ़कर 60, 70, 80 प्रति मिनट हो जाती है। अस्थमा में ब्रोन्कियल नलिकाएं ऐंठनयुक्त हो जाती हैं। वे अनुबंध करते हैं. इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है. प्राणायाम इन नलिकाओं की ऐंठन या सिकुड़न को दूर करता है। एक छोटी झिल्लीदार चपटी टोपी स्वरयंत्र की ऊपरी सतह को ढकती है। इसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। यह भोजन के कणों या पानी को श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। यह एक सुरक्षा वाल्व का कार्य करता है।
जब भोजन का एक छोटा कण श्वसन मार्ग में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो खांसी आती है और कण बाहर निकल जाता है।
फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त अपनी धमनी यात्रा में शुरू होता है, चमकदार-लाल और जीवन देने वाले गुणों और गुणों से भरपूर। यह शिरापरक मार्ग से लौटता है, खराब, सिस्टम के अपशिष्ट पदार्थों से भरा हुआ। धमनियां नलिकाएं या वाहिकाएं होती हैं जो शुद्ध ऑक्सीजनयुक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। नसें वाहिकाएं या नलिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त वापस ले जाती हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध शिरापरक रक्त होता है। हृदय के दाहिनी ओर से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। यह फेफड़ों की लाखों छोटी-छोटी वायु-कोशिकाओं में वितरित होता है। हवा की एक सांस अंदर ली जाती है और हवा की ऑक्सीजन फेफड़ों की बाल जैसी रक्त वाहिकाओं की पतली दीवारों के माध्यम से अशुद्ध रक्त के संपर्क में आती है जिन्हें फुफ्फुसीय केशिकाएं कहा जाता है। केशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं। वे मलमल के कपड़े या छलनी की तरह होते हैं। खून आसानी से निकल जाता है या निकल जाता है। ऑक्सीजन इन पतली केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से प्रवेश करती है। जब ऑक्सीजन ऊतकों के संपर्क में आती है तो एक प्रकार का दहन होता है।
रक्त ऑक्सीजन लेता है और अपशिष्ट उत्पादों और जहरीले पदार्थों से उत्पन्न कार्बोनिक एसिड गैस छोड़ता है, जो सिस्टम के सभी हिस्सों से रक्त द्वारा एकत्र किया गया है। शुद्ध रक्त को चार फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएँ अलिंद तक और वहाँ से बाएँ निलय तक ले जाया जाता है। वेंट्रिकल से इसे सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी में पंप किया जाता है। महाधमनी से यह शरीर की विभिन्न धमनियों में चला जाता है। अनुमान है कि एक दिन में 35,000 पिंट रक्त शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों की केशिकाओं में प्रवेश करता है।
धमनियों से शुद्ध रक्त पतली केशिकाओं में जाता है। केशिकाओं से रक्त की लसीका बाहर निकलती है, शरीर के ऊतकों को स्नान कराती है और उनका पोषण करती है। ऊतक श्वसन ऊतकों में होता है। ऊतक ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अशुद्धियाँ शिराओं द्वारा हृदय के दाहिनी ओर ले जाई जाती हैं।
इस नाजुक संरचना का निर्माता कौन है? क्या आप इन अंगों के पीछे ईश्वर का अदृश्य हाथ महसूस कर रहे हैं? इस शरीर की संरचना निस्संदेह भगवान की सर्वज्ञता का संकेत देती है। अंतर्यामी या हमारे हृदय का वासी द्रष्टा के रूप में आंतरिक कारखाने के कामकाज की निगरानी करता है। उनकी उपस्थिति के बिना, हृदय धमनियों में रक्त पंप नहीं कर सकता। फेफड़े रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं कर पाते। प्रार्थना करना। उन्हें अपनी मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसे हर समय याद रखें. शरीर की सभी कोशिकाओं में उसकी उपस्थिति महसूस करें।
भावार्थ :- सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा व केवली ये आठ प्रकार के कुम्भक अर्थात् प्राणायाम कहे
भावार्थ :- यह सहित कुम्भक दो प्रकार से किया जाता है । एक सगर्भ और दूसरा निगर्भ । सगर्भ कुम्भक को बीजमन्त्र के उच्चारण के साथ व निगर्भ को बिना बीजमन्त्र का उच्चारण करे किया जाता है ।
भावार्थ :- अब मैं पहले सगर्भ प्राणायाम की विधि को कहता हूँ । पहले साधक को किसी भी सुखासन में बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना चाहिए । इसके बाद उसे रजोगुण की प्रधानता वाले लाल रंग से युक्त ‘अकार’ बीजमन्त्र का ध्यान करना चाहिए ।
इसके बाद बुद्विमान साधक उसका (अकार बीजमंत्र का ) सोलह बार जप करते हुए इडा नाड़ी ( बायीं नासिका ) से प्राणवायु को शरीर के अन्दर भरें और श्वास को अन्दर भरने के बाद व उसे अन्दर ही रोकने से ठीक पहले उड्डीयान बन्ध का अभ्यास करना चाहिए ।
अब श्वास को अन्दर भरने के बाद सत्वगुण प्रधान विष्णु के काले रंग से युक्त ‘उकार’ बीजमन्त्र का ध्यान करते हुए उसका चौसठ बार जप करते हुए उस प्राणवायु को शरीर के अन्दर ही रोके रखें ।
इसके बाद पुनः तमोगुण प्रधान शिव और शुक्ल वर्ण से युक्त ‘मकार’ बीजमन्त्र का ध्यान करते हुए उसका बत्तीस बार जप करते हुए उसे दूसरी ( दायीं ) नासिका से बाहर निकाल दें ।
विशेष :- इस सगर्भ प्राणायाम से सम्बंधित कई प्रश्न बनते हैं । जैसे- सगर्भ प्राणयाम करते हुए पहले किस नाड़ी अथवा नासिका से श्वास को भरना चाहिए ? जिसका उत्तर है इडा नाड़ी अथवा बायीं नासिका से । कितनी बार तक मन्त्र का जप करते हुए प्राण को अन्दर भरना चाहिए ? उत्तर है सोलह बार तक । प्राणवायु को अन्दर भरते हुए किस बीजमन्त्र का ध्यान करना चाहिए ? उत्तर है अकार बीजमन्त्र का ।
प्राणवायु को कितने बीजमन्त्र का जप करते हुए अन्दर ही रोकना चाहिए ? उत्तर है चौसठ तक । कुम्भक के समय किस बीजमन्त्र का ध्यान करना चाहिए ? उत्तर है उकार का ।
प्राणवायु को दायीं नासिका से छोड़ते हुए कितने बीजमंत्रों का जप करना चाहिए व किस बीजमन्त्र का जप करना चाहिए ? उत्तर है बत्तीस बार मकार का ।
उड्डीयान बन्ध का अभ्यास कब- कब करना चाहिए ? उत्तर है प्राण को अन्दर भरने के बाद व अन्दर ही रोकने से ठीक पहले ।
भावार्थ :- अब इसके बाद फिर पहले जैसे ही क्रम अथवा प्रकार से ( जिस प्रकार बायीं नासिका से किया गया था ) किया गया था । ठीक उसी प्रकार दायीं नासिका से प्राणवायु को सोलह बीजमन्त्र का उच्चारण करते हुए शरीर के अन्दर भरें व चौसठ बार बीजमन्त्र का जप करते हुए उसे शरीर के अन्दर ही रोके रखें । इसके बाद उसी प्रकार बायीं नासिका से उस प्राणवायु को बत्तीस बीजमंत्र का जप करते हुए बाहर निकाल देना चाहिए ।
भावार्थ :- प्राणायाम के तीन मुख्य अंग होते हैं जिनसे प्राणायाम पूर्ण होता है । रेचक, ( श्वास को बाहर निकालना ) पूरक ( श्वास को अन्दर भरना ) व कुम्भक ( श्वास को अन्दर या बाहर कहीं भी रोक कर रखना ) । इसमें कुम्भक के दो प्रकार होते हैं – एक सहित कुम्भक व दूसरा केवल कुम्भक । जब तक साधक को केवल कुम्भक में सिद्धि नहीं मिल जाती तब तक उसे सहित कुम्भक का अभ्यास करते रहना चाहिए ।
विशेष :- इस श्लोक में प्राणायाम के तीन अंगों की चर्चा की गई है । जिनसे प्राणायाम पूरा होता है । बिना रेचक, पूरक व कुम्भक के कोई भी प्राणायाम पूर्ण नहीं हो सकता ।
सहित कुम्भक
भावार्थ :- जब प्राणायाम को रेचक व पूरक के साथ किया जाता है तब वह सहित कुम्भक कहलाता है ।
विशेष :- सहित कुम्भक में रेचक व पूरक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है । तभी वह सहित कुम्भक कहलाता है ।
केवल कुम्भक
भावार्थ :- रेचक व पूरक के बिना अपने आप प्राणवायु को सुखपूर्वक शरीर के अन्दर धारण करने ( रोकना ) को ही केवल कुम्भक प्राणायाम कहते हैं ।
विशेष :- केवल कुम्भक का अभ्यास रेचक व पूरक के बिना ही किया जाता है ।
केवल कुम्भक की सिद्धि का महत्त्व
भावार्थ :- बिना रेचक व पूरक के केवल कुम्भक प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर योगी साधक के लिए इन तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ अर्थात अप्राप्य नहीं रहता । अर्थात तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर सकते हों ।
केवल कुम्भक द्वारा राजयोग प्राप्ति
भावार्थ :- केवल कुम्भक द्वारा जब साधक पूर्ण सामर्थ्यवान हो जाता है तब वह जब तक चाहे तब तक प्राणवायु को अपने भीतर रोक कर रख सकता है । ऐसा करने से वह राजयोग अर्थात समाधि को भी प्राप्त कर सकता है । इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है ।
केवल कुम्भक के द्वारा कुण्डलिनी जागरण व हठयोग सिद्धि
भावार्थ :- केवल कुम्भक से कुण्डलिनी का जागरण हो जाता है और कुण्डलिनी के जागृत होने से सुषुम्ना नाड़ी के सभी मल रूपी अवरोध भी स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं । इस प्रकार साधक को हठयोग में सिद्धि की प्राप्ति होती है ।
राजयोग व हठयोग का सम्बन्ध
भावार्थ :- हठयोग के बिना राजयोग की व राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए जब तक निष्पत्ति अर्थात समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए ।
विशेष :- इस श्लोक में राजयोग व हठयोग की एक दूसरे पर निर्भरता को दर्शाया गया है । इससे हमें पता चलता है कि यह एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित हैं ।
भावार्थ :- कुम्भक के द्वारा प्राणवायु को पूरी तरह से रोक लेने के बाद साधक को चाहिए कि वह अपने चित्त को आश्रय रहित बना ले । इस प्रकार के योग का अभ्यास करने से साधक को राजयोग के पद की प्राप्ति होती है ।
हठ सिद्धि के लक्षण
भावार्थ :- हठ सिद्धि के लक्षण बताते हुए कहा है कि शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, अनाहत नाद का स्पष्ट रूप से सुनाई देना, नेत्रों का निर्मल हो जाना, शरीर से रोगों का अभाव हो जाना, बिन्दु पर विजय प्राप्त होना या नियंत्रण होना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, नाड़ियो का पूरी तरह से शुद्ध हो जाना, ये सब हठयोग की सिद्धि के लक्षण हैं ।
विशेष :- इस श्लोक में हठयोग में सिद्धि प्राप्त हो जाने से शरीर में प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन किया गया है । परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्त्वपूर्ण श्लोक है ।
भावार्थ :- इस प्रकार यह श्री सहजानन्द परम्परा के महान अनुयायी योगी स्वात्माराम द्वारा रचित हठप्रदीपिका ग्रन्थ में प्राणायाम की विधि बताने वाले कथन नामक दूसरा उपदेश पूर्ण हुआ ।
मानसिक प्रभाव

Powered by Triveni Yoga Foundation

Powered by Triveni Yoga Foundation