3. आसन
स्थिरसुखमासनम्।।2.46।।
(स्थिर-सुखम् आसनम्)
शब्दार्थ=:> शरीर की स्थिति विशेष जिसमें शरीर बिना हिले- डुले स्थिर व सुखपूर्वक देर तक बैठा रह सकता है, उस अवस्था को आसन कहते हैं ।
ये योगासन के नाम से प्रख्यात हैं| आम जनता का विश्वास है कि योगशास्त्र माने योगासन ही हैं। परन्तु वास्तव में योगासन योगशास्त्र के प्रमुख अंश मात्र हैं। योगासन शारीरिक शुद्धि, अवयवों की पुष्टि तथा दीर्घायु में सहयोग देनेवाले साधन हैं। योगासनों के द्वारा रोगों को रोका जा सकता है| रोग आ जाये तो उन्हें दूर भी किया जा सकता है।
पतंजलि के अनुसार, `स्थिरं सुखं आसनं’ अर्थात् सुख से एक ही स्थिति में स्थिर रहना आसन है। आम तौर पर मनुष्य अपने अवयवों को एक ही स्थिति में ज्यादा समय नहीं रख सकता | इसीलिए अवयवों को अलगअलग स्थितियों में रख कर उन्हें सुविधा के अनुसार फैला कर या मोड कर रोगों से मुक्त रहने का प्रयास आदमी करता है। आसनों का लक्ष्य अवयवों को शक्ति एवं सामथ्र्य प्रदान करना है।
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्।।2.47
शब्दार्थ :- प्रयत्न ( सभी शारीरिक गतिविधियों या सभी प्रकार की शारीरिक कोशिशों को )
शैथिल्य ( शिथिल कर देना या रोक देना )
अनन्त ( जिसका कभी अन्त नहीं होता अर्थात ईश्वर या परमात्मा में )
समापत्तिभ्याम् ( पूरा ध्यान लगाने से आसन में सिद्धि मिलती है । )
बिना जल्दबाजी के अभ्यास कर एकाग्र होकर शक्ति के अनुसार, योगासन करना जरूरी है। योगासनों की संख्या बहुत ज्यादा है।
आसन में सिद्धि प्राप्त होने पर हमें क्या फल प्राप्त होता है । इसकी व्याख्या अगले सूत्र में की गई है ।
ततो द्वन्द्वानभिघात: ।। 48 ।।
शब्दार्थ :- तत: ( तब अर्थात आसन की सिद्धि होने पर ) द्वन्द्व ( सर्दी – गर्मी ) भूख- प्यास, लाभ- हानि आदि ) अनभिघात ( आघात अर्थात कष्ट नहीं पहुँचाते )
आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक को सर्दी- गर्मी, भूख- प्यास, लाभ- हानि आदि द्वन्द्व आघात अर्थात कष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं ।
4. प्राणायाम
तस्मिन्सतिश्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः।।2.49।।
तस्मिन् सति-आसन की सिद्धि हो जाने पर
श्वास -प्राणवायु को अन्दर लेने (पूरक) व
प्रश्वासयो: -प्राणवायु को बाहर छोड़ने की (रेचक)
गतिविच्छेद: -सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना ही
प्राणायाम: -प्राणायाम कहलाता है ।
प्राणायाम में प्राण और आयाम दो शब्द हैं। प्राण क्या है ? शक्ति या सांस ही प्राण है। आयाम क्या है ? बढ़ाना या विस्तार करना ही आयाम है| अर्थात् प्राणशक्ति को बढ़ाना या नियंत्रित करना प्राणायाम है | प्राणायाम के विधान अनेक हैं।
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्यामि परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः।।2.50।।
बाह्यवृत्ति: -प्राणवायु को बाहर निकालकर कर बाहर ही रोकना
आभ्यंतर वृत्ति: -प्राणवायु को भीतर भरकर भीतर ही रोकना
स्तम्भवृत्ति:-प्राणवायु को न भीतर भरना न ही बाहर छोड़ना अर्थात प्राणवायु जहाँ है उसे वहीं पर रोकना
देश -स्थान अर्थात प्राणवायु नासिका से जितनी दूरी तक जाता है वह उसका स्थान है।
काल -समय अर्थात जितने समय तक प्राणवायु बाहर या भीतर रुकता है।
संख्याभि: -एक प्राणायाम को करने में स्वाभाविक रूप से कितने श्वास प्रश्वास हो सकते हैं, उनकी गणना द्वारा
परिदृष्ट: -भली प्रकार देखा व जाना हुआ प्राण
दीर्घ -लम्बा व
सूक्ष्म: -हल्का हो जाता है
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः।।2.51।।
शब्दार्थ :- 3बाह्य ( श्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही रोकना )
आभ्यन्तर ( श्वास को अन्दर लेकर अन्दर ही रोकना )
विषय ( कार्य या कर्म का )
आक्षेपी ( त्याग या विरोध करने वाला )
चतुर्थ: ( यह चौथा प्राणायाम है । )
सूत्रार्थ :- श्वास को बाहर रोकने व अन्दर रोकने के विषय अर्थात कार्य का त्याग या विरोध करने वाला यह चौथा प्राणायाम है ।
अगर प्राणायाम सही ढंग से कर सके तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हम स्वयं ही कर सकते हैं। मन अपने काबू में रहेगा। कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा |
5. प्रत्याहार
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।।2.54।
शब्दार्थ :- स्वविषय ( अपने- अपने विषयों अर्थात कार्यों के साथ )
असम्प्रयोगे ( जुड़ाव या सम्बन्ध न होने से )
चित्तस्य- स्वरूपानुकार ( चित्त के वास्तविक स्वरूप के )
इव ( समान या अनुसार )
इन्द्रियाणाम् ( इन्द्रियों का भी वैसा ही हो जाना )
प्रत्याहार: ( प्रत्याहार कहलाता है । )
मन एवं बुद्धि दोनों को शांत कर, उन्हें निर्मल, निश्चल एवं व्यवस्थित बनाये रखना ही प्रत्याहार कहलाता है | प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त करें तो इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। एकाग्रता साध कर मन तपस्या के मार्ग पर चल सकता है।
ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्।।2.55।।
शब्दार्थ :- तत: ( उसके बाद अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि होने पर )
परमा ( परम अर्थात सबसे ऊँचा )
वश्यता ( वशीकरण अर्थात नियंत्रण )
इन्द्रियाणाम् ( इन्द्रियों पर आता है ।)
6. धारणा
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा।।3.1।।
शब्दार्थ :- चित्तस्य ( चित्त को ) देश ( किसी एक स्थान पर ) बन्ध: ( बाँधना अर्थात ठहराना या केन्द्रित करना ) धारणा ( धारणा होती है । )
किसी एक विषय पर एकाग्रता हासिल करना ही धारणा कहलाता है।
हृदय, भूकुटि, जिह्वा, नासिका तथा नाभि वगैरह स्थूल एवं सूक्ष्म विषयों के साथ इष्ट देवी देवता या इष्ट चिह्न व मंत्र पर मन को एकाग्र करना भी धारणा है|
आहार – विहार, बर्ताव, दैनिक कार्यों में सात्विक परिवर्तन कर सकें तो साधक धारण शक्ति की वृद्धि कर सकते हैं।
7. ध्यान
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्।।3.2।।
शब्दार्थ :- तत्र ( जहाँ पर अर्थात जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है उसी स्थान पर )
प्रत्यय ( ज्ञान या चित्त की वृत्ति की )
एकतानता ( एकतानता अर्थात एकरूपता बनी रहना ही )
ध्यानम् ( ध्यान है । )
तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधिः।।3.3।।
शब्दार्थ :- तदेव ( तब वह अर्थात ध्यान ही ) अर्थमात्र ( केवल उस वस्तु के अर्थ या स्वरूप का ) निर्भासं ( आभास करवाने वाला ) स्वरूपशून्यम् ( अपने निजी स्वरूप से रहित हुआ ) इव ( जैसा ) समाधिः ( समाधि होती है । )
प्रत्यय ( ज्ञान या चित्त की वृत्ति की )
एकतानता ( एकतानता अर्थात एकरूपता बनी रहना ही )
ध्यानम् ( ध्यान है । )
8. समाधि
त्रयमेकत्र संयमः।।3.4।।
शब्दार्थ :- त्रयम् ( तीनों अर्थात धारणा, ध्यान व समाधि का )
एकत्र ( एक ही विषय में प्रयोग होना )
संयम: ( संयम होता है । )
अवरोधों तथा रुकावटों को पार कर एक ही विषय पर चित्त को लगाना उसी में लीन होना समाधि कहलाता है| ध्यान की चरम स्थिति ही समाधि है। ध्यान और समाधि की स्थिति में अंतर है। ध्यान में, ध्यान करने वाला, ध्यान से संबंधित विषय तथा ध्यान का लक्ष्य तीनों अलग-अलग रहते हैं। पर समाधि में ये तीनों एक हो जाते हैं।
तज्जयात्प्रज्ञालोकः।।3.5।।
शब्दार्थ :- तत् ( उस अर्थात संयम पे ) ज्यात् ( जय अर्थात विजय प्राप्त करने पर ) प्रज्ञा ( बुद्धि का ) आलोक:, ( प्रकाश या विकास होता है । )
आत्म साक्षात्कार और आत्मा एवं परमात्मा का मिलन ही समाधि का एक मात्र लक्ष्य है। ऊपर बताये गये सातों अंग के अभ्यास की परिणती समाधि है
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः।।3.7।।
शब्दार्थ :- पूर्वेभ्य: ( पूर्व अर्थात पहले कहे गए की अपेक्षा ) त्रयम् ( ये तीन अर्थात धारणा, ध्यान व समाधि ) अन्तरङ्गंम् ( अन्तरङ्ग अर्थात ज्यादा निकट हैं । )
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य।।3.8।।
शब्दार्थ :- तदपि ( वह भी अर्थात धारणा, ध्यान व समाधि भी )
निर्बीजस्य ( निर्बीज अथवा असम्प्रज्ञात समाधि के )
बहिरङ्गं ( बाहरी साधन हैं । )

उपयुक्त योग वेल अष्टांग हमारे देशकी प्राचीन संस्कृति के द्वारा विश्व को प्रदत्त वरदान हैं। हर व्यक्ति का कत्र्तव्य है कि वह इन्हें समझें । निरंतर अभ्यास करें और अपना जीवन चरितार्थ करें।
वपुः कृशत्वं, वदने प्रसन्नता, नाद-स्फुटत्वं, नयने सुनिर्मले,
अरोगता, बिन्दुजयम्, अग्निदीपनं, नाडी विशुद्धिर्हठसिद्धि लक्षणम् ।
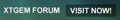






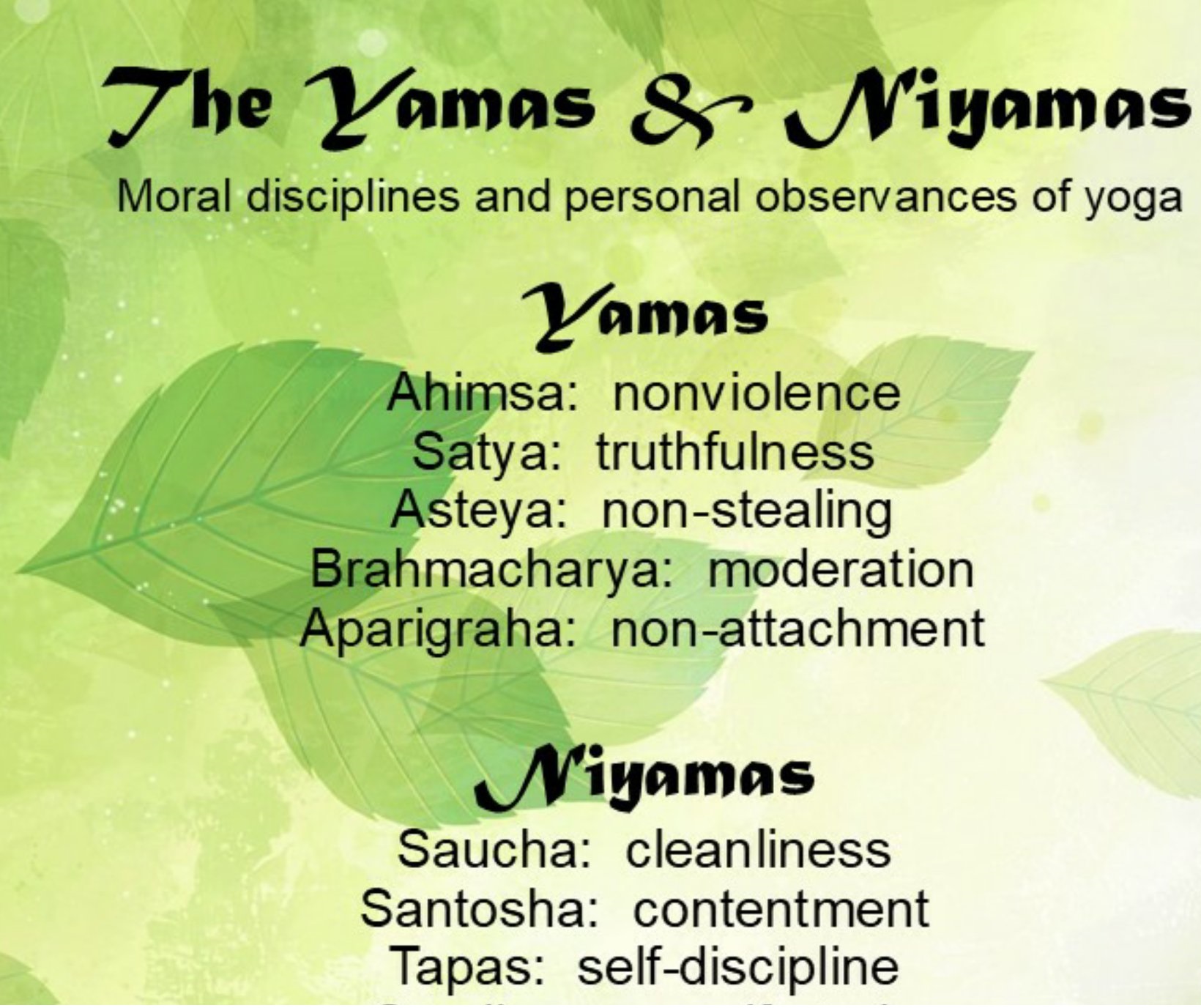
![]()
