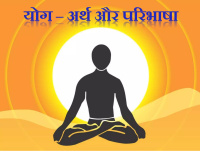1. पातंजल योग दर्शन के अनुसार- योगष्चित्तवृत्ति निरोध: अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है।
2. महर्षि पतंजलि-
‘योगष्चित्तवृत्तिनिरोध:’ यो.सू.1/2
अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य, अन्त:करण से है। बाह्मकरण ज्ञानेन्द्रियां जब विषयों का ग्रहण करती है, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुँचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते है। इस सम्पूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिम्ब बनता है, वही वृत्ति कहलाता है।
यह चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है। अत: विषय उसमें आकर प्रतिबिम्बत होता है अर्थात् चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है।
योग के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने आगे कहा है-
‘तदा द्रश्टु: स्वरूपेSवस्थानम्।। 1/3
अर्थात योग की स्थिति में साधक (पुरूष) की चित्तवृत्ति निरू़द्धकाल में कैवल्य अवस्था की भाँति चेतनमात्र (परमात्म ) स्वरूप रूप में स्थित होती है।
महर्षि पतंजलि ने योग को दो प्रकार से बताया है- 1. सम्प्रज्ञात योग 2.असम्प्रज्ञात योग सम्प्रज्ञात योग में तमोगुण गौणतम रूप से नाम रहता है। तथा पुरूष के चित्त में विवेक-ख्याति का अभ्यास रहता है। असम्प्रज्ञात योग में सत्त्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का परिणाम होना बन्द हो जाता है तथा पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है।
3. सांख्य दर्शन के अनुसार-
पुरुशप्रकृत्योर्वियोगेपि योगइत्यमिधीयते।
अर्थात् पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है।
4. महर्षि याज्ञवल्क्य -
‘संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो।’
अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है।
कठोशनिषद् में योग के विषय में कहा गया है-
‘यदा पंचावतिश्ठनते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिष्च न विचेश्टति तामाहु: परमां गतिम्।।
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभावाप्ययौ।। कठो.2/3/10-11
अर्थात् जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को ‘परमगति’ कहते है। इन्द्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती है, अर्थात् प्रमाद हीन हो जाता है। उसमें सुभ संस्कारो की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। यही अवस्था योग है।
5. मैत्रायण्युपनिषद् -
एकत्वं प्राणमनसोरिन्द्रियाणां तथैव च.।
सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते।। 6/25
अर्थात प्राण, मन व इन्द्रियों का एक हो जाना, एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्म विषयों से विमुख होकर इन्द्रियों का मन में और मन आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना योग है।
6. योगषिखोपनिषद् -
योSपानप्राणयोरैक्यं स्वरजोरेतसोस्तथा। सूर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनो:।
एवंतु़द्वन्द्व जालस्य संयोगो योग उच्यते।। 1/68-69
अर्थात् अपान और प्राण की एकता कर लेना, स्वरज रूपी महाशक्ति कुण्डलिनी को स्वरेत रूपी आत्मतत्त्व के साथ संयुक्त करना, सूर्य अर्थात् पिंगला और चन्द्र अर्थात् इड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन योग है।
7. लिंड्ग पुराण के अनुसार -
लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने योग का लक्षण किया है कि -
सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्यते।
अर्थात् आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। उक्त परिभाषा में भी पुराणकार का अभिप्राय योगसिद्ध का फल बताना ही है। समस्त विषयों को प्राप्त करने का सामर्थ्य योग की एक विभूति है। यह योग का लक्षण नहीं है। वृत्तिनिरोध के बिना यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता।
8. अग्नि पुराण के अनुसार -
अग्नि पुराण में कहा गया है कि
आत्ममानसप्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति:तस्या ब्रह्मणि संयोग योग इत्यभि धीयते।। अग्नि पुराण (379)25
अर्थात् योग मन की एक विशिष्ठ अवस्था है जब मन मे आत्मा को और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है।
संयोग का अर्थ है कि ब्रह्म की समरूपता उसमे आ जाती है। यह कमरूपता की स्थिति की योग है। अग्नि पुराण के इस योग लक्षण में पूवेक्ति याज्ञवल्क्य स्मृति के योग लक्षण से कोई भिन्नता नहीं है। मन का ब्रह्म के साथ संयोग वृत्तिनिरोध होने पर ही सम्भव है।
9. स्कन्द पुराण के अनुसार -
स्कन्द पुराण भी उसी बात की पुष्टि कर रहा है जिसे अग्निपुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति कह रहे है। स्कन्द पुराण में कहा गया है कि-
यव्समत्वं द्वयोरत्र जीवात्म परमात्मनो:।
सा नष्टसर्वसकल्प: समाधिरमिद्यीयते।।
परमात्मात्मनोयोडयम विभाग: परन्तप।
स एव तु परो योग: समासात्क थितस्तव।।
यहां प्रथम “लोक में जीवात्मा और परमात्मा की समता को समाधि कहा गया है तथा दूसरे “लोक में परमात्मा और आत्मा की अभिन्नता को परम योग कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि समाधि ही योग है। वृत्तिनिरोध की ‘अवस्था में ही जीवात्मा और परमात्मा की यह समता और दोनो का अविभाग हो सकता है। यह वात नष्टसर्वसंकल्प: पद के द्वारा कही गयी है।
10. हठयोग प्रदीपिका के अनुसार -
योग के विषय में हठयोग की मान्यता का विशेष महत्व है, वहां कहा गया है कि-
सलिबे सैन्धवं यद्वत साम्यं भजति योगत:।
तयात्ममनसोरैक्यं समाधिरभी घीयते।। (4/5) ह0 प्र0
अर्थात् जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है ; उसी प्रकार जब मन वृत्तिशून्य होकर आत्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेता है तो मन की उस अवस्था का नाम समाधि है। यदि हम विचार करे तो यहां भी पूर्वोक्त परिभाषा से कोई अन्तर दृष्टिगत नही होता। आत्मा और मन की एकता भी समाधि का फल है। उसका लक्षण नही है। इसी प्रकार मन और आत्मा की एकता योग नही अपितु योग का फल है।