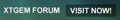



पाँचवा अध्याय ( कुम्भक / प्राणायाम वर्णन )
पाँचवा अध्याय ( कुम्भक / प्राणायाम वर्णन ) पाँचवें अध्याय में मुख्य रूप से आठ प्रकार के प्राणायामों ( कुम्भकों ) की चर्चा की गई है । प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक के शरीर में लघुता अर्थात् हल्कापन आता है । इस अध्याय में प्राणायाम के अतिरिक्त अन्य कई विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है । जिनमें कुछ निम्न हैं – योग करने के लिए उपयुक्त स्थान, कुटिया के लक्षण, काल अर्थात् समय, मिताहार, पथ्य- अपथ्य आहार व नाड़ी शुद्धि आदि ।प्राणायाम वर्णन
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यद्विधिम् । यस्य साधनमात्रेण देवतुल्यो भवेन्नर: ।। 1 ।।
भावार्थ :- इसके बाद ( प्रत्याहार के बाद ) अब प्राणायाम की जो विधि है, मैं उसका अच्छी प्रकार से वर्णन करूँगा । जिसकी साधना मात्र ( केवल जिसके अभ्यास ) से ही मनुष्य देवताओं के समान हो जाता है ।
आदौ स्थानं तथा कालं मिताहारं तथा परम् । नाड़ीशुद्धिं तत: पश्चात् प्राणायामं च साधयेत् ।। 2 ।।
भावार्थ :- साधक पहले स्थान तथा समय उसके बाद मिताहार और फिर नाड़ीशुद्धि को जानकर उनका पालन करे । उसके बाद ही उसे प्राणायाम की साधना का अभ्यास करना चाहिए । विशेष :- इस श्लोक में प्राणायाम की साधना करने से पहले साधक को कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया है । जिनको परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि प्राणायाम की साधना से पूर्व साधक को किन- किन अंगों की साधना करनी चाहिए ? या प्राणायाम से पहले जिन तत्त्वों का अभ्यास आवश्यक होता है, उनका सही क्रम क्या है ? जिसका उत्तर है पहले साधना के लिए उपयुक्त स्थान का निर्णय फिर उपयुक्त समय का निर्णय । इसके बाद मिताहार का पालन और अन्त में साधक को नाड़ीशुद्धि का अभ्यास करना चाहिए । इसके बाद ही उसे प्राणायाम की साधना करनी चाहिए ।
योग साधना के लिए वर्जित स्थान
दूरदेशे तथारण्ये राजधान्यां जनान्तिके । योगारम्भं न कुर्वीत कृतश्चेत् सिद्धि न भवेत् ।। 3 ।। अविश्वासं दूरदेशे अरण्ये रक्षिवर्जितम् । लोकारण्ये प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत् ।। 4 ।।
भावार्थ :- साधक को निम्न स्थानों पर योग के अभ्यास को आरम्भ नहीं करना चाहिए :- कहीं दूर स्थान पर अर्थात् अपने घर से बहुत दूर, जंगल अथवा वन में, बड़े नगरों में अर्थात् भीड़ – भाड़ वाले स्थानों पर जहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हों । इन स्थानों पर योग करने से साधक को कभी भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । दूर देश में अविश्वास का भाव रहता है, जंगल अथवा वन में सुरक्षा की चिन्ता होती है । भीड़- भाड़ वाले स्थान पर बहुत लोगों परिचय करना चाहेंगे । जिससे जनसङ्ग नामक बाधक तत्त्व बढ़ेगा । अतः साधक को कभी भी इन तीनों स्थानों पर योग साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए । यह योग साधना हेतु वर्जित स्थान माने गए हैं । विशेष :- परीक्षा में इस श्लोक के विषय में पूछा जा सकता है कि साधक को किन- किन स्थानों पर योग के अभ्यास को प्रारम्भ नहीं करना चाहिए ? जिसका उत्तर है दूर देश में, जंगल अथवा वन में, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में अर्थात् जहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हों ।
योग करने हेतु उपयुक्त स्थान
सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरूपद्रवे । कृत्वा कुटीरं तत्रैकं प्राचीरै: परिवेष्टितम् ।। 5 ।। वापीकूपतडागं च प्राचीरंमध्यवर्ति च । नात्युच्चं नीतिनिम्नं च कुटीरं कीटवर्जितम् ।। 6 ।। सम्यग्गोमयलिप्तं च कुटीरं तत्रनिर्मितम् । एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामं समभ्यसेत् ।। 7 ।।
भावार्थ :- योग साधना के लिए उपयुक्त स्थान के विषय में बताते हुए कहा है कि योग साधक को योग साधना का अभ्यास निम्न स्थानों पर करना चाहिए :- जो स्थान धार्मिक हो अर्थात् जहाँ का राजा नीतिपूर्ण कार्य करता हो, जहाँ पर साधक को आसानी से भिक्षा ( भोजन आदि ) प्राप्त हो सके, जहाँ पर किसी प्रकार के उपद्रव न होते हो अर्थात् जहाँ पर हिंसक आन्दोलन आदि न होते हों । वहाँ पर एक छोटी कुटिया जो चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई हो । जहाँ पर पानी का कुँआ या तालाब हो, वहाँ की जो भूमि हो वह न तो अधिक ऊँची हो और न ही ज्यादा नीची हो अर्थात् समतल भूमि होनी चाहिए । कुटिया पूरी तरह से कीट- पतंगों ( साँप, बिच्छु आदि ) से बिलकुल रहित होनी चाहिए । वह कुटिया अच्छी प्रकार से गोबर ( गाय के गोबर से ) लिपि होनी चाहिए । इस प्रकार से बने हुए गुप्त अथवा सुरक्षित स्थान पर ही साधक को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । विशेष :- परीक्षा में इससे सम्बंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साधक को किस प्रकार के स्थान पर प्राणायाम अथवा योग साधना का अभ्यास करना चाहिए ? या योग साधक की कुटिया के क्या लक्षण होते हैं ? जिसका उत्तर है साधक की कुटिया धार्मिक स्थान पर, जहाँ भिक्षा आसानी से मिल सके, जो स्थान दंगो से रहित हो, कुटिया चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई हो, अन्दर पानी का कुँआ या तालाब हो, भूमि समतल हो, कीट- पतंगों से रहित हो व अच्छी तरह से गोबर से लिपि हो ।
योगाभ्यास के लिए वर्जित काल समय
हेमन्ते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतौ तथा । योगारम्भं न कुर्वीत कृते योगो हि रोगाद: ।। 8 ।।
भावार्थ :- साधक को हेमन्त, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में योग साधना का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए । इन ऋतुओं में अभ्यास करने पर रोग होने की सम्भावना बढ़ जाती है । विशेष :- साधक को किन- किन ऋतुओं में योग के अभ्यास को प्रारम्भ नहीं करना चाहिए ? जिसका उत्तर है हेमन्त, शिशिर, ग्रीष्म व वर्षा ऋतुओं में । इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी ऋतुओं में योगाभ्यास वर्जित होता है ? जिसका उत्तर है चार ।
योगाभ्यास के लिए उपयुक्त समय
वसन्ते शरदि प्रोक्तं योगारम्भं समाचरेत् । तथायोगी भवेत् सिद्धो रोगान्मुक्तो भवेद् ध्रुवम् ।। 9 ।।
भावार्थ :- योग साधना के विषय में कहा गया है कि साधक को वसन्त व शरद ऋतु में योग साधना की शुरुआत करनी चाहिए । इस समय पर योग साधना की शुरुआत करने वाला योगी निश्चित रूप से रोग मुक्त व सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है । विशेष :- किन- किन ऋतुओं में योग साधना को प्रारम्भ करना चाहिए ? उत्तर है वसन्त व शरद ऋतुओं में । वसन्त व शरद ऋतुओं में योग साधना प्रारम्भ करने से साधक को क्या लाभ मिलते हैं ? उत्तर है साधक रोग मुक्त व सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ।
ऋतुओं का मास ( महीनों ) से सम्बन्ध
चैत्रादिफाल्गुनान्ते च माघादि फाल्गुननान्तिके । द्वौ द्वौ मासौ ऋतुभागौ अनुभावश्चतुश्चतु: ।। 10 ।।
भावार्थ :- चैत्र मास से फाल्गुन मास के अन्त तक ( जिसमें माघ मास भी आता है ) दो- दो महीनों में एक ऋतु का समय पूरा होता है और चार- चार महीनों तक उन ऋतुओं का प्रभाव रहता है । विशेष :- दो महीने में एक ऋतु का समय बताया गया है । हमारे भारत देश में एक वर्ष में कुल छः ऋतुएँ होती हैं । इससे भी स्पष्ट है कि एक ऋतु का समय दो महीने तक होता है ।
वसन्तश्चैत्र वैशाखौ ज्येष्ठाषाढ़ौ च ग्रीष्मकौ । वर्षा श्रावणभाद्राभ्यां शरदाश्विनकार्तिकौ । मार्गपौषौ च हेमन्त: शिशिरो माघ फल्गुनौ ।। 11 ।।
भावार्थ :- चैत्र और वैशाख मास तक वसन्त ऋतु और ज्येष्ठ व आषाढ़ मास तक ग्रीष्म ऋतु होती है । श्रावण से भाद्रपद अर्थात् भादौ तक वर्षा ऋतु और आश्विन से कार्तिक मास तक शरद ऋतु अर्थात् सर्दी होती है । मार्गशीर्ष से पौष माह तक हेमन्त ऋतु और माघ से फाल्गुन मास तक शिशिर ऋतु होती है । विशेष :- ऊपर वर्णित मास व ऋतु का सम्बन्ध परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है । इसे अच्छे से याद करें । आसानी के लिए अन्त में डायग्राम की सुविधा भी दी जा रही है ।
अनुभावं प्रवक्ष्यामि ऋतुनां च यथोदितम् । माघादिमाधवान्तेषु वसन्तानुभवश्चतु: ।। 12 ।।
भावार्थ :- अब मैं जैसा ऋतुओं के विषय में अनुभव होता है, उसका उपदेश करूँगा । माघ मास से वैशाख मास के अन्त तक चार महीनों वसन्त ऋतु का अनुभव होता है । विशेष :- माघ से वैशाख मास के अन्त तक किस ऋतु का प्रभाव होता है ? उत्तर है वसन्त ऋतु का ।
चैत्रादि चाषाढान्तं च निदाघानुभवश्चतु: । आषाढादि चाश्विनान्तं प्रावृषानुभवश्चतु: ।। 13 ।।
भावार्थ :- इसी प्रकार चैत्र मास से लेकर आषाढ़ मास में चार महीने तक ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है तथा आषाढ़ से आश्विन मास में चार महीने तक वर्षा ऋतु रहती है । विशेष :- चैत्र से आषाढ़ तक किस ऋतु का प्रभाव रहता है ? उत्तर है ग्रीष्म अर्थात् गर्मी का । आषाढ़ मास से आश्विन मास तक किस ऋतु का प्रभाव पड़ता है ? उत्तर है वर्षा ऋतु का ।
भाद्रादिमार्गशीर्षान्तं शरदाऽनुभवश्चतु: । कार्तिकादिमाघमासान्तं हेमन्तानुभवश्चतु: । मार्गादिचतुरो मासान् शिशिरानुभवश्चतु: ।। 14 ।।
भावार्थ :- भाद्रपद मास से मार्ग शीर्ष मास के अन्त तक चार महीने शरद ऋतु का प्रभाव रहता है, कार्तिक मास से माघ मास के अन्त तक चार महीने हेमन्त ऋतु का अनुभव होता है और मार्गशीर्ष मास से फाल्गुन मास तक चार महीने शिशिर ऋतु का प्रभाव रहता है । विशेष :- परीक्षा की दृष्टि से ऊपर वर्णित मास व ऋतुओं का सम्बंध उपयोगी है ।
वसन्ते वापि शरदि योगारम्भं समाचरेत् । तदा योगो भवेत् सिद्धो विनायासेन कथ्यते ।। 15 ।।
भावार्थ :- साधक को योग साधना की शुरुआत वसन्त या शरद ऋतु में करनी चाहिए । ऐसा करने से बिना किसी विशेष प्रयास के ही साधक को योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है । विशेष :- किस – किस ऋतु में योगाभ्यास की शुरुआत करने से स्वयं ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है ? अथवा किस- किस ऋतु में योगाभ्यास शुरू करने से बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप ही सिद्धि की प्राप्ति होती है ? उत्तर है वसन्त व शरद ऋतु में ।
मिताहार की उपयोगिता
मिताहारं विना यस्तु योगारम्भं तु कारयेत् । नानारोगो भवेत्तस्य किञ्चिद्योगो न सिद्धयति ।। 16 ।।
भावार्थ :- जो साधक बिना मिताहार का पालन किये ही योगाभ्यास को शुरू कर देता है । उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं साथ ही उसे योग में नाममात्र सिद्धि भी नहीं मिलती । विशेष :- मिताहार का पालन किये बिना योग करने से क्या- क्या हानि होती हैं ? उत्तर है अनेक प्रकार के रोग व सिद्धि प्राप्त न होना ।
ग्राह्यहार ( ग्रहण अथवा खाने योग्य पदार्थ )
शाल्यन्नं यवपिण्डं वा गोधूमपिण्डकं तथा । मुद्गं माषचणकादि शुभ्रं च तुष वर्जितम् ।। 17 ।। पटोलं पनसं मानं कक्कोलं च शुकाशकम् । द्राढ़िका कर्कटीं रम्भां डुम्बरीं कण्टकण्टकम् ।। 18 ।। आमरम्भां बालरम्भां रम्भादण्डं च मूलकम् । वार्ताकी मूलकं ऋद्धिं योगी भक्षणमाचरेत् ।। 19 ।। बालशाकं कालशाकं तथा पटोलपत्रकम् । पञ्चशाकं प्रशंसीयाद्वास्तूकं हिलमो चिकाम् ।। 20 ।।
भावार्थ :- ग्राह्य अथवा हितकारी आहार :- हितकारी आहार में महर्षि घेरण्ड ने निम्न खाद्य पदार्थों को रखा है – चावल, जौ का आटा, गेहूँ का आटा, भूसा रहित मूँग, उड़द व चना आदि दालों को अच्छे से साफ करके । परवल, कटहल, कंकोल, करेला, जिमींकंद, अरवी, ककड़ी, केला, गूलर, व चौलाई का शाक । कच्चा केला या केले का डंठल और फूल, केले के बीच का भाग या दण्ड, केले की जड़, बैंगन, मूली आदि का योगी को सेवन करना चाहिए । कच्चा शाक, मौसमी सब्जियाँ, परवल का शाक, बथुआ व हिमलोचिका अर्थात् हुरहुर की सब्जी आदि पाँच प्रकार के शाक को योगी हेतु प्रशंसनीय बताया गया है । विशेष :- हितकारी आहार का अर्थ है जिन खाद्य पदार्थों को ग्रहण अथवा खाना चाहिए । ऐसा आहार जो योग साधना में सहायक हो, जो शीघ्रता से पचने वाले हों । ऊपर वर्णित सभी खाद्य पदार्थ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं ।
मिताहार वर्णन
शुद्धं सुमधुरं स्निग्धं उदरार्द्घविवर्जितम् । भुज्यते सुरसं प्रीत्या मिताहारमिमं विदुः ।। 21 ।।
भावार्थ :- पूरी तरह से शुद्ध अर्थात् स्वच्छ, मधुर अर्थात् मीठा, स्निग्ध अर्थात् घी आदि से बना चिकना भोजन, आधा पेट अर्थात् भूख से आधा भोजन जो शरीर में रस व प्रीति अर्थात् सुख को बढ़ाता है । उसे विद्वानों ने मिताहार कहा हैं । विशेष :- मिताहार के सम्बंध में यही पूछा जाता है कि कौन- कौन से पदार्थों को मिताहार में शामिल किया गया है ? उत्तर है शुद्ध, मीठा, चिकना, भूख से आधा अथवा आधा पेट, रस व सुख को बढ़ाने वाला आहार ।
पेट में भोजन, पानी व वायु की मात्रा वर्गीकरण
अन्नेन पूरयेदर्धं तोयेन तु तृतीयकम् । उदरस्य तुरियांशं संरक्षेद्वायुचारणे ।। 22 ।।
भावार्थ :- पेट के आधे भाग अथवा हिस्से को अन्न से भरें, तीसरे हिस्से को जल से व चौथे हिस्से को वायु के आने- जाने के लिए खाली छोड़ देना चाहिए । विशेष :- परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पेट के कितने हिस्से को अन्न, जल व वायु के लिए सुरक्षित रखना चाहिए ? उत्तर है आधे हिस्से को अथवा दो हिस्सों को अन्न के लिए, तीसरे हिस्से को पानी व चौथे हिस्से को वायु के लिए सुरक्षित रखना चाहिए ।
अग्राह्य आहार ( वर्जित आहार )
कट्वम्लं लवणं तिक्तं भृष्टं च दधि तक्रकम् । शाकोत्कटं तथा मद्यं तालं च पनसं तथा ।। 23 ।। कुलत्थं मसूरं पाण्डुं कुष्माण्डं शाकदण्डकम् । तुम्बीकोलकपित्थं च कण्टबिल्वं पलाशकम् ।। 24 ।। कदम्बं जम्बीरं निम्बं कलुचं लशुनं विषम् । कामरङ्गं प्रियालं च हिङ्गुशाल्मलीकेमुकम् । योगारम्भे वर्जयेत्पथ्यं स्त्रीवह्निसेवनम् ।। 25 ।। नवनीतं घृतं क्षीरं गुड शक्रादि चैक्षवम् । पञ्चरम्भां नारिकेलं दाडिमंमसिवासरम् । द्राक्षां तु नवनीं धात्रीं रसमम्लंविवर्जितम् ।। 26 ।।
भावार्थ :- योगी साधक को निम्न खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए :- कडुआ, खट्टा, नमकीन, तीखा, ज्यादा भुने हुए, दही व छाछ, विरेचक अथवा बुरे शाक, मादक द्रव्यव ( शराब आदि ), ताड़ का फल, लकुच । कुल्थी, मसूर दाल, प्याज, पेठा, दाण्डी का शाक, कड़वी घीया, वेर, कांटे वाली बेल पर पके हुए पलाश के फल- फूल । कदम्ब, जम्बीर नीम्बू, लकुच, लहसुन, किसी भी प्रकार का विष, कमरख, चिरौंजी, हींग, सेमर के फूल, गोभी, लम्बी यात्रा, स्त्री का सङ्ग और अग्नि के सेवन आदि योग के आरम्भ में वर्जित कहे गए हैं । नया घी अर्थात् मक्खन, दूध, गुड़ व शक्कर आदि, पाँच प्रकार के केले के भाग, नारियल, अनार, सौंफ, मुनक्का, खट्टे रस से रहित आँवला व अम्ल रस वाले पदार्थों का सेवन वर्जित है ।
योगी के लिए खाद्य ( खाने योग्य ) पदार्थ
एलाजातिलवङ्गं च पौरुषं जम्बु जाम्बुलम् । हरीतकीं च खर्जूरं योगी भक्षणमाचरेत् ।। 27 ।। लघुपाकं प्रियं स्निग्धं तथा धातुप्रपोषणम् । मनोऽभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत् ।। 28 ।।
भावार्थ :- इलायची, लौंग, पका हुआ फालसा, जामुन, जाम्बुल ( जामुन का मोटा रूप अर्थात् जमोया ), हरड़ व खजूर आदि वस्तुओं का सेवन योगी को करना चाहिए । इसके अतिरिक्त जल्दी पकने वाले पदार्थ, खाने में अच्छे लगने वाले, चिकने, शरीर की सभी धातुओं को पुष्ट करने वाले पदार्थ, मन को अच्छा लगने वाले योग्य खाद्य पदार्थों का ही सेवन योगी को करना चाहिए ।
वर्जित खाद्य ( न खाने अथवा त्यागने योग्य ) पदार्थ
काठिन्यं दुरितं पूतिमुष्णं पर्युषितं तथा । अतिशीतं चातिचोष्णं भक्ष्यं योगी विवर्जयेत् ।। 29 ।।
भावार्थ :- देरी से पकने व पचने वाला, दूषित, सड़ा हुआ, ज्यादा गर्म, ज्यादा ठण्डा अथवा बासी भोजन का सेवन योगी को कभी नहीं करना चाहिए ।
अन्य वर्जित ( न करने योग्य ) कार्य
प्रात: स्नानोपवासादि कायक्लेशविधिं तथा । एकाहारं निराहारं यामान्ते च न कारयेत् ।। 30 ।।
भावार्थ :- योगी द्वारा उन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए जिनके करने से शरीर को कष्ट होता हो । जिनमें प्रातः काल में स्नान, उपवास, एक ही समय भोजन करना, भोजन के बिना ही रहना व सायंकाल के बाद भोजन करना आदि सभी कार्यों को त्याग देना चाहिए ।
प्राणायाम के आरम्भ काल में करने योग्य भोजन
एवं विधिविधानेन प्राणायामं समाचरेत् । आरम्भे प्रथमं कुर्यात् क्षीराज्यं नित्यभोजनम् । मध्याह्ने चैव सायाह्ने भोजनद्वयमाचरेत् ।। 31 ।।
भावार्थ :- इस प्रकार योगी को पूरे विधि- विधान के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । प्राणायाम के आरम्भिक समय में प्रतिदिन दूध और घी से युक्त आहार का सेवन करना चाहिए । इसके अलावा योगी को आरम्भ में दोपहर व सांय दो समय भोजन करना चाहिए ।
नाड़ी शुद्धि वर्णन
कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कम्बले । स्थलासने समासीन: प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुख: । नाड़ीशुद्धिं समासाद्य प्राणायामं समभ्यसेत् ।। 32 ।।
भावार्थ :- प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले योगी को नाड़ीशुद्धि का अभ्यास करना चाहिए । इसके लिए उपयुक्त आसन ( बैठने के स्थान ) बताते हुए कहा है कि साधक को कुश से बने आसन पर, मृग ( हिरण ) के चमड़े से बने आसन पर, व्याघ्र ( शेर ) के चमड़े से बने आसन या फिर कम्बल को बिछाकर उसके ऊपर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके नाड़ीशुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । विशेष :- इस श्लोक से सम्बंधित कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं । जैसे- प्राणायाम करते समय साधक को किस प्रकार के आसन पर बैठना चाहिए ? उत्तर है कुश, मृग ( हिरण ) के चमड़े की खाल पर, शेर की खाल के चमड़े पर और कम्बल पर । प्राणायाम करते समय साधक को किस दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए ? उत्तर है पूर्व और उत्तर दिशा की ओर । या यह भी पूछा जा सकता है कि साधक को किस दिशा की ओर मुख करके प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए ? उत्तर है पश्चिम व दक्षिण दिशा की ओर ।
नाड़ीशुद्धिं कथं कुर्यान्नाड़ीशुद्धिस्तु कीदृशी । तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तद्वदस्व दयानिधे ।। 33 ।।
भावार्थ :- राजा चण्ड कापालिक महर्षि घेरण्ड को कहते हैं कि हे दयानिधे! यह नाड़ी शुद्धि क्या होता है ? और इस नाड़ी शुद्धि को कैसे किया जाता है ? यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ । कृपा आप इसको बताएं ।
मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव गच्छति । प्राणायाम: कथं सिध्येत्तत्त्वज्ञानं कथं भवेत् । तस्मादादौ नाड़ीशुद्धिं प्राणायामं ततोऽभ्यसेत् ।। 34 ।।
भावार्थ :- जब साधक की नाड़ियों में मल ( अवशिष्ट पदार्थ ) भरा होता है तो उस समय प्राणवायु नाड़ियों के अन्दर नहीं पहुँच पाती है । प्राणवायु के अन्दर प्रवेश न कर पाने से प्राणायाम किस प्रकार सिद्ध हो सकता है अर्थात् साधक को प्राणायाम में सफलता कैसे मिलेगी ? और उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे होगी ? इसलिए सबसे पहले साधक को अपनी नाड़ियों की शुद्धि के लिए नाड़ीशुद्धि का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास । विशेष :- इससे सम्बंधित प्रश्न :- साधक को पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए या प्राणायाम का ? उत्तर है नाड़ीशुद्धि का । नाड़ियों में जमा मल को किसके द्वारा साफ अथवा शुद्ध किया जाता है ? उत्तर है नाड़ीशुद्धि द्वारा ।
नाड़ीशुद्धिर्द्विधा प्रोक्ता समनुर्निर्मनुस्तथा । बीजेन समनुं कुर्यान्निर्मनुं धौतकर्मणा ।। 35 ।।
भावार्थ :- यह नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है । एक समनु तथा दूसरी निर्मनु । नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बीजमन्त्र के साथ करने को समनु कहते हैं और बिना मन्त्र के अर्थात् धौतिकर्म के द्वारा करने को निर्मनु कहते हैं । विशेष :- परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण श्लोक है । इसमें पूछा जा सकता है कि नाड़ी शुद्धि के कितने प्रकार कहे गए हैं ? उत्तर है दो ( समनु व निर्मनु ) । समनु को किस विधि से किया जाता है अथवा समनु विधि में किसका प्रयोग किया जाता है ? उत्तर है बीजमन्त्र का । निर्मनु में किस विधि का प्रयोग किया जाता है ? उत्तर है धौतिकर्म का ।
धौतकर्म पुरा प्रोक्तं षट्कर्मसाधने यथा । श्रृणुष्व समनुं चण्ड! नाड़ीशुद्धिर्यथा भवेत् ।। 36 ।।
भावार्थ :- निर्मनु अर्थात् धौतिकर्म के द्वारा नाड़ी शुद्धि किस प्रकार की जाती है ? इसका वर्णन षट्कर्म के अध्याय में पहले ही किया जा चुका है । यहाँ पर समनु अर्थात् बीजमन्त्र के साथ नाड़ी शुद्धि किस प्रकार की जाती है ? इसका वर्णन सुनो ।
उपविश्यासने योगी पद्मासनं समाचरेत् । गुर्वादिन्यासनं कुर्याद् यथैव गुरु भाषितम् । नाड़ीशुद्धिं प्रकुर्वीत प्राणायामविशुद्धये ।। 37 ।।
भावार्थ :- नाड़ीशुद्धि के लिए पहले साधक पद्मासन लगाकर बैठे । इसके बाद गुरुओं को प्रणाम करते हुए उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें ताकि उसके बाद प्राणायाम को अच्छी प्रकार से किया जा सके ।
नाड़ी शुद्धि की विधि
वायुबीजं ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णं सतेजसम् । चन्द्रेण पूरयेद्वायुं बीजै: षोडशकै: सुधी: ।। 38 ।। चतु:षष्टया मात्रया च कुम्भकेनैव धारयेत् । द्वात्रिंशन्मात्रया वायुं सूर्यनाड्या च रेचयेत् ।। 39 ।।
भावार्थ :- बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह धुएँ के जैसे रंग वाले तेजयुक्त वायु के बीजमन्त्र अर्थात् ‘यँ’ का ध्यान करते हुए अपने चन्द्रनाड़ी अर्थात् बायीं नासिका से सोलह ( 16 ) बीजमंत्रो का जाप करते हुए प्राण को शरीर के अन्दर भरे । इसके बाद उस अन्दर भरी हुई प्राणवायु को चौसठ ( 64 ) बीजमंत्रों का जाप करते हुए शरीर के अन्दर ही रोके रखें और अन्त में बत्तीस ( 32 ) बीजमंत्रों का जाप करते हुए उस प्राणवायु को सूर्यनाड़ी अर्थात् दायीं नासिका से बाहर निकाल दें ।
नाभिमूलाद्वह्निमुत्थाप्य ध्यायेत्तेजोऽवनीयुतम् । वह्निबीजषोडशेन सूर्यानाड्या च पूरयेत् ।। 40 ।। चतु:षष्टया मात्रया च कुम्भकेनैव धारयेत् । द्वात्रिंशन्मात्रया वायुं शशिनाड्या च रेचयेत् ।। 41 ।।
भावार्थ :- नाभि के मूल अर्थात् नाभि के बीच में स्थित अग्नि तत्त्व को ऊपर की ओर उठाते हुए अग्नि तत्त्व के स्थान अर्थात् जहाँ पर मणिपुर चक्र स्थित होता है । वहाँ पर अग्नि के बीजमन्त्र ‘रँ’ का ध्यान करते हुए सूर्यनाड़ी अर्थात् दायीं नासिका से सोलह बीजमन्त्रों का जाप करते हुए प्राणवायु को शरीर के अन्दर भरें । फिर उस प्राणवायु को चौसठ बीजमन्त्रों का जाप करते हुए शरीर के अन्दर ही रोके रखें । इसके बाद बत्तीस बीजमंत्रों का जाप करते हुए प्राणवायु को चन्द्रनाड़ी अर्थात् बायीं नासिका से बाहर निकाल दें । विशेष :- नाड़ीशुद्धि की विधि को हम एक बार सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं । नाड़ीशुद्धि करते हुए पहले बायीं नासिका से श्वास को सोलह बीजमंत्रों का जाप करते हुए अन्दर भरते हैं । फिर चौसठ बीजमंत्रों का जाप करते हुए उस प्राणवायु को शरीर के भीतर ही रोका जाता है । इसके बाद उस प्राणवायु को बत्तीस बीजमंत्रों का जाप करते हुए दायीं नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है । यहाँ तक नाड़ी शुद्धि की आधी विधि होती है । इसके बाद इसी विधि को दायीं नासिका से शुरू करते हुए बायीं नासिका पर खत्म कर दिया जाता है । इससे सम्बंधित अनेक प्रश्न बनते हैं । जैसे – नाड़ी शुद्धि करते हुए पहले किस नासिका से प्राणवायु को अन्दर भरा जाता है ? उत्तर है बायीं नासिका से । नाड़ीशुद्धि करते हुए अन्त में किस नासिका से प्राणवायु को बाहर छोड़ा जाता है ? उत्तर है बायीं नासिका से । नाड़ीशुद्धि करते हुए प्राणवायु को अन्दर लेने, अन्दर रोकने व वापिस बाहर छोड़ने का क्या अनुपात होता है ? उत्तर है 16:64:32 ( 1:4:2 ) । इसे बीजमन्त्र के अनुसार 16:64:32 का अनुपात कहा जाता है और वैसे सामान्य रूप से उसे 1:4:2 का अनुपात कहा जाता है अर्थात् जितने समय तक प्राणवायु को अन्दर भरते हैं उससे चार गुणा समय तक उसे शरीर के अन्दर रोकना और उससे आधे समय में उसे बाहर निकाल देना । इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जा सकता है कि बायीं नासिका अर्थात् चन्द्रनाड़ी से श्वास अन्दर लेते हुए किस तत्त्व का ध्यान करना चाहिए ? उत्तर है वायु तत्त्व का । वायु तत्त्व का बीजमन्त्र क्या होता है ? उत्तर है ‘यँ’ । दायीं नासिका से अर्थात् सूर्यनाड़ी से श्वास को अन्दर भरते हुए किस तत्त्व का ध्यान करना चाहिए ? उत्तर है अग्नि तत्त्व का । अग्नि तत्त्व का बीजमन्त्र क्या होता है ? उत्तर है ‘रँ’ ।
नासाग्रे शशिधृग्बिम्बं ध्यात्वा ज्योत्स्नासमन्वितम् । ठं बीजंषोडशेनैव इडया पूरयेन्मरुत् ।। 42 ।। चतु:षष्टया मात्रया च वं बीजेनैव धारयेत् । अमृतं प्लावितं ध्यात्वा नाड़ीधौतं विभावयेत् । लकारेण द्वात्रिंशेन दृढं भाव्यं विरेचयेत् ।। 43 ।।
भावार्थ :- नासिका के अग्रभाग अर्थात् अगले हिस्से पर चन्द्रिका ( चाँदनी से युक्त ) से युक्त चन्द्र तत्त्व का ध्यान करते हुए ‘ठं’ बीजमन्त्र का सोलह बार मानसिक जप करते हुए इडा नाड़ी ( बायीं नासिका ) से श्वास को अन्दर भरें । उसके बाद ‘वं’ बीजमन्त्र का चौसठ बार मानसिक जप करते हुए उस प्राणवायु को शरीर के अन्दर ही रोके रखें और नाड़ी मण्डल में अमृत को निरन्तर धारण करने व उसके साथ ही नाड़ीधौति की भावना करनी चाहिए । इसके बाद बत्तीस बार ‘लं’ बीजमन्त्र का मानसिक जप करते हुए प्राणवायु को पिङ्गला नाड़ी ( दायीं नासिका ) से बाहर निकाल दें ।
एवं विधां नाड़ीशुद्धिं कृत्वा नाड़ी विशोधयेत् । दृढ़ो भूत्वासनं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत् ।। 44 ।।
भावार्थ :- इस प्रकार विधिपूर्वक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करके अपनी सभी नाड़ियों की भली प्रकार से शुद्धि करें । इसके बाद साधक को दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । विशेष :- साधक को प्राणायाम का अभ्यास किसके बाद करना चाहिए ? उत्तर है नाड़ी शुद्धि के बाद ।
सहित: सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा । भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्टकुम्भिका: ।। 45 ।।
भावार्थ :- सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा व केवली ये आठ प्रकार के कुम्भक अर्थात् प्राणायाम कहे गए हैं । विशेष :- इस श्लोक में घेरण्ड संहिता में वर्णित आठ प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है । परीक्षा में इनकी प्राणायामों के प्रकार, इनका क्रम आदि पूछा जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जा सकता है कि घेरण्ड संहिता में कितने प्राणायाम ऐसे हैं जिनका वर्णन हठ प्रदीपिका में नहीं किया गया है ? उत्तर है दो ( सहित कुम्भक व केवली कुम्भक ) ।
सहित कुम्भक वर्णन
सहितो द्विविध: प्रोक्त: सगर्भश्चनिगर्भक: । सगर्भो बीजमुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जित: ।। 46 ।।
भावार्थ :- यह सहित कुम्भक दो प्रकार से किया जाता है । एक सगर्भ और दूसरा निगर्भ । सगर्भ कुम्भक को बीजमन्त्र के उच्चारण के साथ व निगर्भ को बिना बीजमन्त्र का उच्चारण करे किया जाता है । विशेष :- परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सहित कुम्भक के कितने प्रकार हैं ? उत्तर है दो ( सगर्भ व निगर्भ ) । कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसकी दो विधियाँ हैं या किस प्राणायाम के दो प्रकार कहे गए हैं ? उत्तर है सहित कुम्भक । किस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए बीजमन्त्र का प्रयोग अथवा उच्चारण किया जाता है ? उत्तर है सगर्भ कुम्भक । सहित कुम्भक के किस अभ्यास में बीजमन्त्र का उच्चारण नहीं किया जाता ? उत्तर है निगर्भ ।
सगर्भ प्राणायाम विधि वर्णन
प्राणायामं सगर्भं च प्रथमं कथयामि ते । सुखासने चोपविश्य प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुख: । ध्यायेद्विधिं रजोगुणं रक्तवर्णमवर्णकम् ।। 47 ।। इडया पूरयेद्वायुं मात्रया षोडशै: सुधी: । पूरकान्ते कुम्भकाद्ये कर्तव्यस्तूड्डीयानक: ।। 48 ।। सत्त्वमयं हरिंध्यात्वा उकारं कृष्णवर्णकम् । चतु:षष्टया च मात्रया कुम्भकेनैव धारयेत् ।। 49 ।। तमोमयं शिवं ध्यात्वा मकारं शुक्लवर्णकम् । द्वात्रिंशन्मात्रया चैव रेचयेद्विधिना: पुनः ।। 50 ।।
भावार्थ :- अब मैं पहले सगर्भ प्राणायाम की विधि को कहता हूँ । पहले साधक को किसी भी सुखासन में बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना चाहिए । इसके बाद उसे रजोगुण की प्रधानता वाले लाल रंग से युक्त ‘अकार’ बीजमन्त्र का ध्यान करना चाहिए । इसके बाद बुद्विमान साधक उसका (अकार बीजमंत्र का ) सोलह बार जप करते हुए इडा नाड़ी ( बायीं नासिका ) से प्राणवायु को शरीर के अन्दर भरें और श्वास को अन्दर भरने के बाद व उसे अन्दर ही रोकने से ठीक पहले उड्डीयान बन्ध का अभ्यास करना चाहिए । अब श्वास को अन्दर भरने के बाद सत्वगुण प्रधान विष्णु के काले रंग से युक्त ‘उकार’ बीजमन्त्र का ध्यान करते हुए उसका चौसठ बार जप करते हुए उस प्राणवायु को शरीर के अन्दर ही रोके रखें । इसके बाद पुनः तमोगुण प्रधान शिव और शुक्ल वर्ण से युक्त ‘मकार’ बीजमन्त्र का ध्यान करते हुए उसका बत्तीस बार जप करते हुए उसे दूसरी ( दायीं ) नासिका से बाहर निकाल दें । विशेष :- इस सगर्भ प्राणायाम से सम्बंधित कई प्रश्न बनते हैं । जैसे- सगर्भ प्राणयाम करते हुए पहले किस नाड़ी अथवा नासिका से श्वास को भरना चाहिए ? जिसका उत्तर है इडा नाड़ी अथवा बायीं नासिका से । कितनी बार तक मन्त्र का जप करते हुए प्राण को अन्दर भरना चाहिए ? उत्तर है सोलह बार तक । प्राणवायु को अन्दर भरते हुए किस बीजमन्त्र का ध्यान करना चाहिए ? उत्तर है अकार बीजमन्त्र का । प्राणवायु को कितने बीजमन्त्र का जप करते हुए अन्दर ही रोकना चाहिए ? उत्तर है चौसठ तक । कुम्भक के समय किस बीजमन्त्र का ध्यान करना चाहिए ? उत्तर है उकार का । प्राणवायु को दायीं नासिका से छोड़ते हुए कितने बीजमंत्रों का जप करना चाहिए व किस बीजमन्त्र का जप करना चाहिए ? उत्तर है बत्तीस बार मकार का । उड्डीयान बन्ध का अभ्यास कब- कब करना चाहिए ? उत्तर है प्राण को अन्दर भरने के बाद व अन्दर ही रोकने से ठीक पहले ।
सगर्भ प्राणायाम की पूरक विधि
पुनः पिङ्गलयापूर्य कुम्भकेनैव धारयेत् । इडया रेचयेत् पश्चात् तद् बीजेन क्रमेण तु ।। 51 ।।
भावार्थ :- अब इसके बाद फिर पहले जैसे ही क्रम अथवा प्रकार से ( जिस प्रकार बायीं नासिका से किया गया था ) किया गया था । ठीक उसी प्रकार दायीं नासिका से प्राणवायु को सोलह बीजमन्त्र का उच्चारण करते हुए शरीर के अन्दर भरें व चौसठ बार बीजमन्त्र का जप करते हुए उसे शरीर के अन्दर ही रोके रखें । इसके बाद उसी प्रकार बायीं नासिका से उस प्राणवायु को बत्तीस बीजमंत्र का जप करते हुए बाहर निकाल देना चाहिए ।
प्राणायाम के समय किन- किन अँगुलियों का प्रयोग करें
अनुलोमविलोमेन वारं वारं च साधयेत् । पूरकान्ते कुम्भकांते धृतनासापुटद्वयम् । कनिष्ठानामिकाङ्गुष्ठै: तर्जनीमध्यमे विना ।। 52 ।।
भावार्थ :- अनुलोम – विलोम अर्थात् बायीं और दायीं नासिका से इस श्वसन प्रक्रिया को बार- बार करना चाहिए । ऐसा करते हुए प्राण को शरीर में भरते हुए व शरीर से बाहर निकालते हुए नासिका के दोनों ओर कनिष्ठा, अनामिका ( सबसे छोटी, तीसरी ) अँगुलियों व अँगूठे का ही प्रयोग करें । तर्जनी व मध्यमा ( पहली व दूसरी ) अँगुलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । विशेष :- परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्राणायाम साधना के दौरान किन- किन अँगुलियों का प्रयोग करना चाहिए ? जिसका उत्तर है कनिष्ठा ( सबसे छोटी ) व अनामिका ( तीसरी या रिंग फिंगर ) व अँगूठे का ही प्रयोग करना चाहिए । या यह भी पूछा जा सकता है कि अनुलोम- विलोम साधना2 करते हुए किन- किन अँगुलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ? जिसका उत्तर है तर्जनी ( पहली ) व मध्यमा ( दूसरी अथवा सबसे बड़ी ) अँगुलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।
निगर्भ प्राणायाम वर्णन
प्राणायामो निगर्भस्तु विना बीजेन जायते । एकादिशतपर्यन्तं पूरककुम्भकरेचनम् ।। 53 ।।
भावार्थ :- निगर्भ प्राणायाम को बिना बीजमन्त्र के ही किया जाता है । साधक को पूरक ( श्वास को अन्दर भरना ), कुम्भक ( प्राण को अन्दर ही रोके रखना ) और रेचक ( प्राण को बाहर निकालना ) क्रियाओं को एक से सौ बार ( 100 ) तक बिना बीजमन्त्र के करना चाहिए । विशेष :- निगर्भ प्राणायाम करते हुए पूरक, कुम्भक व रेचक क्रियाओं को कितनी बार करना चाहिए ? उत्तर है एक सौ बार ( 100 )
प्राणायाम की उत्तम, मध्यम व निकृष्ट अवस्थाएँ
उत्तमा विंशतिर्मात्रा षोडशी मात्रा मध्यमा । अधमा द्वादशी मात्रा प्राणायामास्त्रिधा स्मृता: ।। 54 ।।
भावार्थ :- गुणवत्ता के आधार पर प्राणायाम के तीन विभाग बनाये गए हैं । जिनमें बीस मात्रा वाले प्राणायाम को उत्तम अर्थात् सबसे अच्छा माना जाता है । सोलह मात्रा वाले प्राणायाम को मध्यम अर्थात् बीच वाला माना जाता है और बारह मात्रा वाले प्राणायाम को अधम अर्थात् निकृष्ट या कम अच्छा माना जाता है । विशेष :- यहाँ पर मात्रा का अर्थ प्राणायाम करते हुए किये गए समय होता है । प्राणायाम में पूरक, कुम्भक व रेचक का सामान्य अनुपात 1: 4: 2 होता है । जिसमें एक का अर्थ है श्वास को अन्दर भरने में जितना समय लगता है वह एक अनुपात कहलाता है । दूसरा कुम्भक होता है चार अनुपात अर्थात् जितने समय प्राण को अन्दर भरते हुए लगा है उससे चार गुणा अधिक समय तक उसे शरीर के अन्दर ही रोके रखना । उसके बाद तीसरा होता है रेचक जिसका अनुपात दो होता है । जिसका अर्थ है जितने समय में प्राण को अन्दर भरा था, उससे दुगने समय तक उसे बाहर निकालना । अब यहाँ पर कही गई मात्रा को समझते हैं । इसमें बीस मात्रा को उत्तम माना गया है । बीस मात्रा वाले प्राणायाम का अर्थ होता है बीस बीजमन्त्र तक प्राण को अन्दर भरना फिर उसे अस्सी मात्रा अर्थात् बीजमन्त्र का जप करते हुए अन्दर ही रोके रखना और फिर चालीस मात्रा अर्थात् चालीस बीजमंत्रों तक उसे बाहर निकालना । इसे हम और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं । जब प्राणवायु को अन्दर भरते हुए हम बीस सैकेंड लगाते हैं और उसे अस्सी सैकेंड तक अन्दर ही रोके रखते हैं फिर उसके बाद चालीस सैकेंड तक उस प्राणवायु को बाहर छोड़ने में लगाते हैं । यह बीस मात्रा ( 20: 80: 40 ) वाला प्राणायाम हुआ । जिसे सबसे उत्तम माना जाता है । इसके बाद इसी प्रकार सोलह मात्रा वाले को बीच वाला ( 16: 64: 32 ) व बारह मात्रा ( 12: 48: 24 ) वाले को अधम या निकृष्ट माना जाता है । परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी श्लोक है ।
उत्तम, मध्यम व निकृष्ट अवस्था के लक्षण
अधमाज्जायते धर्मो मेरुकंपं च मध्यमात् । उत्तमाच्च भूमित्यागस्त्रिविधंसिद्धिलक्षणम् ।। 55 ।।
भावार्थ :- अधम प्रकार का प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है जिससे पसीना उत्पन्न होता है । मध्यम प्रकार का प्राणायाम से मेरुदण्ड अर्थात् रीढ़ की हड्डी में कम्पन उत्पन्न होने लगती है और उत्तम प्रकार का प्राणायाम करने से साधक का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगता है । इस प्रकार यह तीन प्रकार के साधकों की सिद्धि के अलग- अलग लक्षण होते हैं । विशेष :- इससे सम्बंधित प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि उत्तम प्रकार का प्राणायाम करने से साधक में किस प्रकार का लक्षण प्रकट होता है ? उत्तर है जमीन से ऊपर उठने का अर्थात् भूमि त्याग करने का । मध्यम श्रेणी के साधक में किस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है ? उत्तर है मेरुदण्ड में कम्पन का । अधम प्रकार के साधक का क्या लक्षण होता है ? उत्तर है ज्यादा पसीना आना ।
सहित प्राणायाम के लाभ
प्राणायामात् खेचरत्त्वं प्राणायामाद् रोगनाशनम् । प्राणायामाद् बोधयेच्छक्तिं प्राणायामान्मनोन्मनी । आनन्दो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत् ।। 56 ।।
भावार्थ :- प्राणायाम साधना करने से साधक को आकाश में विचरण अर्थात् घूमने की शक्ति की प्राप्ति होती है, उससे सभी रोग समाप्त होते हैं, कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है, समाधि की सिद्धि होती है, चित्त में विशेष प्रकार का सुख अथवा आनन्द का अनुभव होता है इसके अतिरिक्त प्राणायाम करने वाला साधक सदा सुखी रहता है । विशेष :- ऊपर वर्णित सभी लाभ महत्वपूर्ण हैं । विद्यार्थी इन्हें याद रखें ।
Join Us On Social Media
Last Date Modified
2024-08-05 16:40:29Your IP Address
216.73.216.24
Your Your Country

Total Visitars
14Powered by Triveni Yoga Foundation